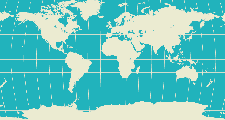पत्रकारिता पर अहंकार और अज्ञानता का साया
 गंभीर चुनौतियों के सामने अख़बार
गंभीर चुनौतियों के सामने अख़बार

अरविंद कुमार सिंह
आधुनिक प्रौद्योगिकी ने मीडिया की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। आज मीडिया की पहुंच समाज के हर वर्ग तक है। इसी नाते उसे और जिम्मेदार रहने की जरूरत हो गयी है। समय का तकाजा है कि मीडिया बहुत संयम से चले, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। टीवी पत्रकारिता की तरह अखबारों के सामने भी कई चुनौतियां दिख रही हैं। खास तौर पर खबरों की होड़ के चलते अखबारी पत्रकारिता भी प्रभावित हो रही है और विश्वसनीयता का गंभीर संकट नजर आ रहा है। अखबारों के लिए यही संतोष का विषय हो सकता है कि आज भी उनकी साख खिसकी नहीं है। आज भी छपे शब्द पर जितना भरोसा लोग करते हैं, किसी और माध्यम पर नहीं। इसी नाते इतने चैनलों के आने के बाद भी अखबार अपनी जगह न सिर्फ कायम है बल्कि उनका विस्तार हो रहा है। पर दबाव में अखबारों को अपना रूप-रंग और कलेवर बदलना पड़ रहा है। खबरों के तरीके भी बदल रहे हैं।
भाषाई पत्रकारिता पर भी बाजारवाद लगातार अपना रंग दिखा रहा है। भारत की सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंसी इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने 2003-04 में भारत के कुछ प्रमुख शहरों में अखबारी पाठकों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर एक सर्वेक्षण किया। इसमें सवाल पूछा गया कि अगर आपको पूरे महीने भर के लिए अखबार या टीवी में से कोई एक चुनने को कहा जाये तो आप किसे चुनेंगे? शत प्रतिशत लोगों का जवाब था कि वे अखबार को चुनेगें क्योंकि टीवी के बिना तो रहा जा सकता है पर अखबार के बिना नहीं।
लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। अखबारों की दुनिया भी नयी हवा में बदल रही है। कुछ अखबारों में भी पेज 3 नाम की नयी संस्कृति में धनाढ्य लोगों की पार्टियों और उनके डांस कार्यक्रमों का विशद चित्रण दिखाया जा रहा है, तो कुछ जगहों पर परिशिष्टों में मिर्च मसाले के साथ अर्धनग्न तस्वीरें परोसने की होड़ है। अखबारों को चुनिंदा खास वर्गो तक बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग चल रहे हैं, पर क्षेत्रीय अखबारों मे भी गांवो की खबरें नदारद होती है। खेतीबाड़ी से जुड़े तमाम गंभीर सवाल मीडिया से बाहर हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प जनहित याचिका दायर की गयी जिसमें मांग की गयी थी कि अखबारों को उनके विषय के आधार पर वर्गीकृत किया जाये। याची का कहना था कि अखबारों में फिल्मों की तरह ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किस आयुवर्ग को कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए। अगर दर्शकों को यह पता होता है कि फिल्में किस आयुवर्ग के लिए बनी हैं तो पाठकों को भी ऐसा पता होना चाहिए। नाबालिको के सामाने अश्लील सामग्री की भरमार को देखते हुए दिशानिर्देश जारी करने की मांग भी की गयी। यह मांग खुद में काफी गंभीर है और अखबारों को आत्ममंथन को विवश करती है।
तमाम लोग यह तर्क देते हैं कि लोग राजनीति और अपराधों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अखबार या चैनल क्या करें? पर वास्तविकता यह है कि अखबारों और चैनलों ने ही ज्यादा स्पेस देकर इसे पाठकों की रूचि का विषय बना दिया है। पहले राजनीतिक दलों, सरकारों और सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर करने वाली स्टोरी प्रमुखता पाती थी पर आजकल या तो तारीफ या फिर आलोचना और उसमें भी निजी हमले की स्टोरी ज्यादा दिखती है। कई जगहों पर राजनीतिक अपराधियों और सीधे अपराधियों से पत्रकारों की सांठगांठ है और वे प्रेस की आड़ लेते हैं।
समाचार माध्यमों को गांव और गरीबों की चिंता कहीं नही नजर आती है। देश में आज भी 102 करोड़ लोगों में से 26 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं जबकि 10 करोड़ बिल्कुल कगार पर खड़े है और उनको संभाला न गया तो वे भी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे। उनके बुनियादी सवालों को नजरंदाज करके हम कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं। इसी तरह से मनमाना लेखन हो रहा है। बिहार में लालू यादव की जगह जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो एक पत्रिका ने राबड़ी सरकार को पेटीकोट सरकार करार दिया। ऐसी नयी शब्दावली और नयी व्याख्या करने वाले भूल जाते हैं कि हर चीज के कुछ बुनियादी मापदंड हैं। यही लोग जब किसी डाकू को बागी या दस्यु सम्राट या फिर दस्यु सुंदरी लिख कर संबोधित करते हैं तो उनका महिमामंडन और आतंक दोनो खुलेआम दिखता है।
पहले संपादकों की स्वीकृति के बिना अखबारों में विज्ञापन नहीं छपते थे। पर आज किसी भी संपादक को यह पता नही होता कि कौन सा विज्ञापन छप रहा है। अखबारों में छपने वाली हर वस्तु के लिए पीआरबी एक्ट के तहत संपादक जिम्मेदार है, पर प्रबंधन ने बिना संपादकों को भरोसे में लिए किसी भी तरह के विज्ञापनों के प्रकाशन की परंपरा सी बना ली है। इसी तरह 70 के दशक तक दंगो या जातीय झगड़ों में मीडिया बहुत संयम बरतता था और खबरों में गुटों या समुदायों का ही जिक्र किया जाता था। पर अब खुलेआम हिंदू-मुसलमान, हरिजन और यादव लिखने में संकोच नहीं किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भोपाल कांड और पनवारी और कुम्हेर (राजस्थान) के जाट-जाटव दंगों में मीडिया ने सीधे जातियों का नाम देकर कवरेज किया और यहां दंगे रोकने के लिए सेना तक की मदद लेनी पड़ी। गांवो में दंगें बहुत मामूली बात पर हुए थे और मीडिया ने इनको और भड़का दिया। पंजाब का आतंकवाद सिख आतंकवाद बन गया और कश्नीर का आतंकवाद मुसलिम आतंकवाद। 1989-92 के बीच तो विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को आसमान तक उठाने के पीछे मीडिया के अधकचरे तत्व ही जिम्मेदार थे। उन्होने ऐसा सांप्रदायिक उन्माद फैलाया कि उसकी परिणति में बाबरी मस्जिद ध्वंश हो गया। मगर जब इन्ही तत्वों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट को तो उनका मोहभंग हुआ। पर तब तक कितनी देर हो चुकी थी यह उनको पता है।
पत्रकार को समाज का आईना माना जाता है। एक समर्पित पत्रकार समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के प्रति स्वंय सजग रह कर शासन,प्रशासन और समुदाय के समस्त यथार्थ का अन्वेषण करता है। स्वच्छ पत्रकारिता से ही किसी सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा की जा सकती है। अगर कोई पत्रकार लोकभावना को भूल जाये तो पत्रकारिता की आत्मा पर ही वह कुठाराघात करता है। पत्रकारिता और आजीविकाओं जैसी नही है और न इसे वैभव के लिए हथियार बनाया जाना चाहिए। खुद सरकारों ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और समाज ने पत्रकारों को अपना दर्पण अनायास नहीं माना है। इस संबोधन के पीछे का दायित्वबोध पत्रकारों को होना ही चाहिए।
चिंता का एक अहम पक्ष यह भी है कि पत्रकारिता में अहंकार और अज्ञानता काफी बढ़ रही है। पत्रकार खुद को विशिष्ट जमात में शामिल करते हुए वीआईपी समझने लगे हैं। वे आम आदमी से लगातार कटते जा रहे हैं और शासन और ताकत के आसपास ही मंडराते नजर आते हैं। मीडिया को भी कई संस्थान फिल्म उद्योग जैसे ग्लैमर में डुबा रहे हैं। मीडिया को किसी संस्था की छवि धूमिल करके उसे रातों रात कटघरे में खड़ा करने में संकोच नहीं होता है। तमाम पत्रकारों को पढ़ने लिखने या किसी विषय में विशेषज्ञता में कोई दिलचस्पी नहीं है और मीडिया के अनुसंधान का पक्ष बहुत अंधेरा है। कई बड़े समूहों में पुस्तकालय तक नहीं है तो ऐसे में वे अनुसंधान और विकास पर क्या खर्च करेंगे इसकी सहज कल्पना की जा सकती है।
अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन ने 1950 में एक आचार संहिता स्वीकारने का फैसला किया था। इसके बाद कई और पत्रकार संस्थाओं ने भी ऐसी पहल की। संपादक सम्मेलन की आचार संहिता में प्रमुख बातें इस प्रकार थीं-
समाचार देते समय पत्रकार न्यायनिष्ट रहें।
जातीय, धार्मिक और आर्थिक मामलों पर लिखते समय विशेष सावधानी और निष्पक्षता बरती जाये
समाचारों में तथ्यों को तोडा मरोड़ा न जाये न कोई सूचना छिपायी जाये।
व्यावसायिक गोपनीयता का निष्ठा से अनुपालन
पत्रकारिता के माध्यम से व्यक्तिगत हितों का पोषण न करें।
पत्रकार अपने पद और पहुंच का उपयोग गैर पत्रकारीय कार्यो के लिए न करें।
रिश्वत लेकर समाचार छापना या न छापना अवांछनीय, अमर्यादित और अनैतिक है।
किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अफवाह फैलाने के लिए पत्रकारिता का उपयोग नहीं किया जाये। यह पत्रकारिता की मर्यादा के खिलाफ है। अगर ऐसा समाचार छापने के लिए जनदबाव हो तो भी पत्रकार पर्याप्त संतुलित रहे।
कुछ साल पहले राष्ट्रपति एपीजे अव्दुल कलाम के हस्ताक्षर से एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने एक पत्रकार व्यवहार संहिता भी जारी की थी। इसमें भी काफी मनन के बाद कई बिंदुओं को शामिल किया गया था। कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-
पर्याप्त समय सीमा के तहत पीड़ित पक्ष को अपना जवाब देने या खंडन करने का मौका दें।
किसी व्यक्ति के निजी मामले को अनावश्यक प्रचार देने से बचें।
किसी खबर में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उसमें अतिश्योक्ती से बचें।
निजी दुख वाले दृश्यों से संबंधित खबरों को मानवीय हित के नाम पर आंख मूंद कर न परोसा जाये। मानवाधिकार और निजी भावनाओं की गोपनीयता का भी उतना ही महत्व है।
धार्मिक विवादों पर लिखते समय सभी संप्रदायों और समुदायों को समान आदर दिया जाना चाहिए।
अपराध मामलो में विशेषकर सेक्स और बच्चों से संबंधित मामले में यह देखना जरूरी है कि कहीं रिपोर्ट ही अपने आप में सजा न बन जाये और किसी जीवन को अनावश्यक बर्बाद न कर दे।
चेकबुक जर्नलिस्म या फिर पैसा लेकर सूचना लेना पाप की कमाई की तरह है। ऐसा कोई विकल्प नहीं बचने पर ही करना चाहिए,पर भुगतान स्वीकृत वैध रूप से किया जाये और वित्तीय पत्रकारिता को बाजार के साथ खिलवाड़ के साथ मिश्रित नहीं किया जाये।
चोरी छिपे सुनकर (और फोटो लेकर) किसी यंत्र का सहारा लेकर ,किसी के निजी टेलीफोन पर बातचीत को पकड़ कर ,अपनी पहचान छिपा कर या चालबाजी से सूचनाएं प्राप्त नहीं की जायें। सिर्फ जनहित के मामले में ही जब ऐसा करना उचित हो और सूचना प्राप्त करने का कोई और विकल्प न बचा हो तो ऐसा किया जाये।
महात्मा गांधी खुद एक प्रखर पत्रकार थे। उन्होने दलितों के बारे में 1945 में लिखा था कि पूर्व में भी पश्चिम की तरह अखबार बाईबिल, कुरान और गीता बनते जा रहे हैं। अखबार में जो कुछ छपता है, उसे लोग ईश्वरीय सत्य मान लेते हैं। इस नाते संपादकों और अन्य पत्रकारों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद 23 अप्रैल 1947 को हरिजन में उन्होने लिखा-प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा सकता है। उसके शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस शक्ति का दुरूपयोग करना एक अपराध है। मैं स्वयं एक पत्रकार हूं और साथी पत्रकारों से अपील करता हूं कि अपने उत्तरदायित्वों को समझें और अपना काम करते समय केवल इस विचार को प्रश्रय दें कि सच्चाई को सामने लाना है और उसी का पक्ष लेना है।
भारत में प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता कायम रखने और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार लाने के लिए की गयी थी। पर नयी चुनौतियों से निपटने के लिए इसके पास साधन और अधिकार नही है। इसी के साथ इलेक्ट्रानिक मीडिया जिस तरह से गैरजिम्मेदाराना शैली में चल रहा है, उस पर खास चिंता जताने के बाद आम राय यही बनी कि सरकार को प्रेस परिषद या संचार आयोग के बजाय मीडिया काउंसिल बनानी चाहिए। 11 नवंबर 2000 को मीडिया काउंसिल के बारे में सरकार के पास प्रस्ताव परिषद की ओर से भेजा गया था। 17 मार्च 2004 की प्रेस परिषद की बैठक में कहा गया कि मीडिया की सभी शाखाओं के निरीक्षण के लिए मीडिया काउंसिल स्थापित की जाये और इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया की दो अलग-अलग शाखाएं बनायी जायें। पर यह प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में ही पड़ा रह गया।
पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गयी थी। देश में प्रेस के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के साथ प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए काम करती है। पर नयी चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिकार संपन्न बनाए जाना जरूरी है। परिषद के निर्देशों को स्वीकारने से अखबार कतराने लगे हैं। उसके पास केवल निंदा करने तक का अधिकार है जिससे काम नहीं बनने वाला है। इलेक्ट्रानिक मीडिया जिस तरह से गैरजिम्मेदाराना शैली में चल रहा है। वह खास चिंता का विषय है। इसे भी दायरे में लेने के लिए व्यापक अधिकार संपन्न मीडिया काउंसिल का गठन जरूरी हो गया है।
मीडिया के लोग हमेशा सभी वर्गो से यह अपेक्षा करते हैं कि उनका उच्च स्तर का आचार और व्यवहार हो। सबके लिए वे आचार संहिता की वकालत भी करते हैं, पर जब पत्रकारों के लिए आचार संहिता की बात आती है तो काफी बवाल होने लगता है। सवाल यह उठता है कि आखिर पत्रकारों के लिए आचार संहिता क्यों नहीं हो। आजादी के इतने सालों के बाद भी भारत में पत्रकारों ने कभी अपने आचार संहिता तक की बात नहीं मानी। वैसे तो मीडिया अरसे से राजनेताओं, व्यापारियों, डाक्टरों, वकीलों और उद्योगपतियों के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता और नैतिकता की बार-बार दुहाई देता है पर अपने लिए वह खुद कोई आचार संहिता बनाने से डरता है। तहलका कांड के बाद जब यह खुलासा हुआ कि सच उजागर करने के लिए शराब, धन और वेश्याओं का उपयोग किया गया तो भी पत्रकारिता की आचार संहिता को लेकर सवाल उठे थे।
हाल के स्टिंग आपरेशनों के बाद भी यह बहस तेज हुई पर किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। कारण यह है कि बहुत से पत्रकार और पत्रकार संगठन किसी भी तरह की आचार संहिता का विरोध करते हैं। पर पेशे की गरिमा के प्रति चिंतित ज्यादातर पत्रकार जीवंत आचार संहिता के पैरोकार हैं और इस पर आम सहमति है कि पत्रकार खुद अपने लिए आचार संहिता बनाएं और ठोस मानक खुद तय करें। अगर पत्रकार खुद इस दिशा में सजग हो जाएं तो सरकार कोई कानून थोपने का साहस ही कैसे कर सकती है। दुनिया के कई देशों में ऐसी आचार संहिताएं विद्यमान हैं तो भारत में लक्ष्मणरेखा खींचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता की आचार संहिता हेतु कुछ मापदंड निर्धारित किए थे जिसके तहत अश्लील और फूहड़ सामग्री का प्रकाशन न करने,जनसामान्य की सुरूचि को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री न छापने जैसी बातें कही गयी थी। भारतीय प्रेस परिषद अखबारों में ऐसे प्रकाशनों (जिसमें विज्ञापन भी शामिल हैं) के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है और खुद भी उन पर निगाह रखती है। विज्ञापन के लिए भी आचार संहिता बनी है पर उसका पालन केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी ही करते हैं।

 मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश